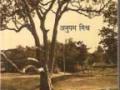अनुपम मिश्र
सरकारी विभागों में भटक कर ‘पुर गये तालाब’
Posted on 27 Oct, 2014 04:42 PMइन तालाबों को अपने आप अपने श्रम से, चंदे से, अपनी सूझबूझ से प

बदली है चाल मेघों की या...
Posted on 06 Jul, 2014 11:02 AM मेघों की चाल से धरती पर जिंदगी की नियति तय होती है। इसी नाते इधर कुछ वर्षों में मौसम के उलटफेर के चलते धरती की आबोहवा में भी कुछ बदलाव दिखने शुरू हुए, तो कहा जाने लगा कि मेघों ने अपनी चाल बदल ली है। लेकिन क्या सचमुच मेघों की चाल बदली है या माजरा कुछ और है? प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और ‘आज भी खरे हैं तालाब’ के चर्चित लेखक के विचार दिलचस्प हैं।बहुत से नेता आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि हमारी खेती भगवान भरोसे है, इसलिए हम पिट जाते हैं। वे कहते हैं कि यह हमारे भरोसे होनी चाहिए और हम विज्ञान से उसको करके दिखा सकते हैं। इसीलिए बड़े-बड़े बांध बनते हैं, फिर उनकी सैकड़ों किलोमीटर की नहरें बनती हैं। वे यह मानते हैं कि मेघ अपनी चाल बदल देंगे, तो हमारे पास उनको अंगूठा दिखाने का एक तरीका है कि हमने भी अपनी चाल इतनी आधुनिक कर ली है कि हम तुमको याद भी नहीं करने वाले और हमारे खेतों में पानी पहुंच जाएगा। अकसर यह कहा जाता है कि अब मेघों ने अपनी चाल बदल दी है। असल में मेघों की चाल बदली या नहीं बदली, यह पक्के तौर पर कहना कठिन है। उससे ज्यादा भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि हमारी चाल जरूर बदल गई है।
पिछले सौ-सवा सौ साल में मौसम विभाग-जैसा कोई विभाग हमारे समाज में, हमारे देश में और दुनिया के विभिन्न देशों में अस्तित्व में आया है। दो- पांच वर्ष का अंतर होगा, लेकिन ऐसी चीजें बहुत पुरानी नहीं हैं। वर्षा, मेघ, पानी का गिरना, आषाढ़ का आना, सावन-भादों- ये सब हजारों साल के अनुभव हैं समाज के, उसके सदस्यों के, विशेषकर किसानों के-जिनका पूरा जीवन इस पर टिका रहता है।
उन्होंने कभी अपनी चाल नहीं बदली, बल्कि मेघों की चाल देखकर अपना व्यवहार तय किया था।

शेर-शेरनी या हम
Posted on 29 Jun, 2014 01:24 PM दिल्ली से निकलने वाले उस समय के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में एक दिन पहले पन्ने पर खबर छपी थी- मध्य प्रदेश के एक बहुत ही दुर्गम इलाके पातालकोट में एक शेर नरभक्षी हो गया है और उसने अब तक छह लोगों को मार डाला है। बड़ा आतंक फैल गया है वहां। अखबार तो प्रसिद्ध था ही, उसके भोपाल स्थित ये संवाददाता भी बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी-अपनी सुंदर जगहों को लोग कुछ तो अपनेपन से, और कुछ घमंड से भी दुनिया का स्वर्ग बताते ही हैं। अक्सर इसके लिए कुछ पहाड़ की, कुछ ऊंचाई की भी जरूरत होती है पर अपनी किसी जगह को पाताल बताने के लिए एक खास तरह की गहराई चाहिए।हमारा परिवार मध्य प्रदेश का है, पर कोई पच्चीस बरस का हो जाने तक भी मुझे पता नहीं था कि मध्य प्रदेश में एक जगह सचमुच पाताल जैसी गहरी है। इसका नाम ही है पातालकोट। छिंदवाड़ा जिले में। इसकी जानकारी और फिर इस पाताल में उतरने का संजोग भी एक विचित्र घटना से मिला था। वे दिन आपात्काल लगने के आसपास के थे। महीना वगैरह तो अब याद नहीं।
दिल्ली से निकलने वाले उस समय के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में एक दिन पहले पन्ने पर खबर छपी थी- मध्य प्रदेश के एक बहुत ही दुर्गम इलाके पातालकोट में एक शेर नरभक्षी हो गया है और उसने अब तक छह लोगों को मार डाला है।

राजरोगियों की खतरनाक रजामंदी
Posted on 13 May, 2014 04:01 PMदूरी छोटा-सा शब्द है, लेकिन जब राज और समाज के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो समाज का कष्ट कितना बढ़ जाता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अच्छे लोग भी जब राज के नजदीक पहुंचते हैं तो उनको विकास का रोग लगा जाता है, भूमंडलीकरण का रोग लग जाता है, उनको लगता है सारी नदियां जोड़ दें, सारे पहाड़ों को समतल कर दें- बुलडोजर चला कर, उनमें खेती कर लेंगे। मात्र यही ख्याल प्रकृति के विरुद्ध है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह प्रभू का काम है, सुरेश प्रभु सहित देश के प्रभु बनने के चक्कर में इसे नेता लोग न करें तो अच्छा है।
नदियां प्रकृति ही जोड़ती है। गंगा कहीं से निकली, यमुना कहीं से निकली। अगर ऊपर हेलिकॉप्टर से देखें तो एक ही पर्वत की चोटी से ठीक नीचे दो बिंदु से दिखेंगे। वहां उनमें गंगोत्री और यमुनोत्री में बहुत दूरी नहीं है। प्रकृति उन्हें वहीं जोड़ देती। लेकिन सब जगह अलग-अलग सिंचाई करके दोनों कहां मिलें, यह प्रकृति ने तय किया था। तब वहां संगम बना। उसके बाद डेल्टा की भी सेवा करनी है नदी को।
‘जब दामोदर नदी पर बांध बन रहा था, तब कपिल भट्टाचार्य नाम के इंजीनियर थे। वे किसी वैचारिक संगठन से नहीं जुड़े थे। लेकिन वे नदी से जुड़े हुए आदमी थे। उन्होंने अपने विभाग से अनुरोध किया कि दामोदर नदी घाटी योजना को रोक लें।
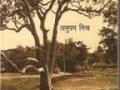
सामाजिक संगठन और प्रबंध
Posted on 22 Feb, 2014 10:57 AM खेतिहर समाज में पानी के प्रबंध का सारा काम ग्राम स्तर पर ही होता रहा है। इसमें तालाब आदि की योजना बनाना, उसके लिए धन और श्रम जुटाना और फिर उसका सतत रख-रखाव करना-इन तीनों स्तरों पर आज जिसे हम ‘जन भागीदारी’ कहते हैं -उसी का पूरा सहारा लिया जाता था। ग्राम सभा या पंचायत के स्तर पर खड़ा यह बुनियादी ढांचा अंग्रेजी राज के दौर से पूरी तरह नष्ट हो गया था। आजादी के बाद उसे कुछ हद तक वापस लाने का प्रयत्न जरूर हुआ पर मोटे तौर पर वह सरकारी पंचायतों के ढांचे में बदल गया था। कोई भी समाज शून्य में नहीं रह सकता। उसे अपने को व्यवस्थित ढंग से चलाने के ढांचे विकसित करने ही पड़ते हैं। इसमें भी यदि समाज का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है तो उस खेतिहर समाज को मिट्टी, पानी, गोबर तथा वनों के ठीक उपयोग का एक सशक्त ढांचा ढालना ही पड़ता है। इन्हीं संसाधनों पर खेतिहर, पशुपालक, समाज टिका रहता है। इसलिए इन ढांचों में कई तरह के और कई स्तर पर लागू हो सकने वाले नियम-कायदे बनाने पड़ते हैं। फिर इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इन नियम-कायदों में न सिर्फ सबकी सहमति हो, सब उन्हें अपने ऊपर लागू करने में भी बिना किसी दबाव के सहर्ष स्वेच्छा से आगे आएं। तब समाज अपनी ठीक गति से, अपनी धुरी पर चलता है, आगे बढ़ता है तथा उत्पादन के साधनों का, प्राकृतिक साधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अपना विकास करता है।समाज को चलाने का यह ढांचा तभी व्यवस्थित हो पाता है जब समाज की नींव से लेकर शिखर तक सब स्तर उसमें शामिल हों। इनमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन जरूर आ सकते हैं, कुछ नीतियां यहां-वहां बदली जा सकती हैं पर उसकी मूलधारा वर्षों के साझे अनुभव से ही संचालित होती है।
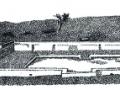
बर्बादी की बाढ़, समझ का अकाल
Posted on 28 Dec, 2013 12:39 PM जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था। कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरि
जल संग्रह की परंपरा
Posted on 21 Dec, 2013 01:45 PM पानी के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा जाता है तो उसका प्रारंभ प्रायः उसे जीवन का आधार बताने से होता है। “जल अमृत है, जल पवित्र है, समस्त जीवों का, वनस्पतियों का जीवन, विकास – सब कुछ जल पर टिका है।” ऐसे वाक्य केवल भावुकता के कारण नहीं लिखे जाते। यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि पानी पर ही हमारे जीवन का, सारे जीवों का आधार टिका है। यह आधार प्रकृति ने सर्व सुलभ, यान
प्रलय का शिलालेख
Posted on 24 Jun, 2013 09:09 PMअबकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण तबाही हुई है। पर बादल, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन आदि को तबाही का कारण मानना कितना सही होगा? इन इलाकों में पीछे हुई घटनाओं से क्या हम कुछ समझना चाहते हैं या नहीं। इन अप्राकृतिक घटनाओं में प्राकृतिक होने की वजहों की छानबीन की ही जानी चाहिए। उत्तराखंड में हिमालय और उसकी नदियों के तांडव का आकार-प्रकार अब धीरे-धीरे बढ़ने और दिखने लगा है। लेकिन क्या सचमुच में मौसमी बाढ़ इस इलाके में नई है? सन् 1977 में अनुपम मिश्र का लिखा एक यात्रा वृतांत।
सन् 1977 की जुलाई का तीसरा हफ्ता। उत्तरप्रदेश के चमोली जिले की बिरही घाटी में आज एक अजीब-सी खामोशी है। यों तीन दिन से लगातार पानी बरस रहा है और इस कारण अलकनंदा की सहायक नदी बिरही का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। उफनती पहाड़ी नदी की तेज आवाज पूरी घाटी में टकरा कर गूंज भी रही है। फिर भी चमोली-बदरीनाथ मोटर सड़क से बाईं तरफ लगभग 22 किलोमीटर दूर 6,500 फुट की ऊंचाई पर बनी इस घाटी के 13 गांवों के लोगों को आज सब कुछ शांत-सा लग रहा है।
आज से सिर्फ सात बरस पहले ये लोग प्रलय की गर्जना सुन चुके थे, देख चुके थे। इनके घर, खेत व ढोर उस प्रलय में बह चुके थे। उस प्रलय की तुलना में आज बिरही नदी का शोर इन्हें डरा नहीं रहा था। कोई एक मील चौड़ी और पांच मील लंबी इस घाटी में चारों तरफ बड़ी-बड़ी शिलाएं, पत्थर, रेत और मलबा भरा हुआ है, इस सब के बीच से किसी तरह रास्ता बना कर बह रही बिरही नदी सचमुच बड़ी गहरी लगती है।

किनारे की मैल से परेशान ना हों
Posted on 20 May, 2013 01:03 PM विनोबा कहते हैं कि पानी तो निकलता है, बहता है समुद्र में मिलने क