
deforestation
जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था। कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी वैसी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, महाविद्यालय तक नहीं था। हमारे यहां एक भी सिविल इंजीनियर नहीं था पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक पश्चिम से पूरब तक कोई 25 लाख छोटे-बड़े तालाब थे। इनसे भी ज्यादा संख्या में जमीन का स्वभाव देखकर अनगिनत कुएं बनाए गए थे। वर्षा का पानी तालाबों में कैसे आएगा, किस तरह के क्षेत्र से, यहां-वहां से बहता आएगा- उसका आगौर अनुभवी आंखों से नाप लिया जाता था। यह प्रसंग करीब 93 बरस पहले का है, जिसका जिक्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने किया है।
अश्विन के महीने में बिहार के छपरा जिले में एक दिन घनघोर बरसात हुई। चौबीस घंटों में लगभग छत्तीस इंच वर्षा हुई, नतीजा यह हुआ कि पूरा जिला भयानक बाढ़ में डूब गया। वहां के सरकारी कर्मचारियों ने लोगों की इस मुसीबत में बहुत ही उदासीनता और उपेक्षा का भाव दिखाया। उन दिनों छपरा से मशरक तक जाने वाली रेल लाइन के कारण बाढ़ का सारा पानी आगे बहने के बदले एक बड़े भाग में फैल गया था और पीछे से आने वाली विशाल धारा उसका स्तर लगातार उठाते जा रही थी। लोगों को इससे बचने का एक ही रास्ता दिखा था, रेलवे लाइन काट देना और चढ़ते पानी को आगे के भूभाग में फैलने देना जहां कुछ सांस ली जा सके। पर कलेक्टर ने उनकी एक न सुनी और तो और ऐसी ही तबाही मचा रही अन्य रेलवे लाइनों पर सशस्त्र पहरा बिठा दिया गया था। सीवान के पास एक ऐसी ही जगह बहुत पानी जमा हो गया था। गांव वालों ने तब खुद ही उस रेल लाइन को काटना तय कर लिया। पर सामने सशस्त्र पुलिस देख उनकी हिम्मत न पड़ी।
राजेंद्र बाबू इसका वर्णन करते हुए लिखते हैः “कष्ट सहते गए लोग। पर जब वह बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दो-चार आदमी कंधे पर कुदाल रखकर पानी में तैरते हुए रेल लाइन की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब दिया कि पानी में डूब कर तो हम मर ही रहे हैं और तुम लाइन नहीं काटने देते। अब तक हमने बर्दाश्त किया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरना दोनों हालत में है। डूब कर मरें या गोली खाकर मरें। हमने निश्चय कर लिया है कि गोली खाकर मरना बेहतर है। हम लाइन काटेंगे, तुम गोली मारो।”
बहते पानी में ये बहादुर लोग तैरते हुए मजबूत बांध की तरह उठी हुई उस रेल लाइन पर अपने दृढ़-निश्चय से कुदाल चलाते गए। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई गोली चलाने की। लाइन अभी थोड़ी-सी ही कट पाई थी कि पीछे भर रहे पानी की ताकत ने लोगों के संकल्प में साथ दिया और लाइन भड़ाक से टूटी और विशाल बाढ़ का पानी उसे किसी तिनके की तरह अपने साथ न जाने कहां बहा ले गया। पीछे के अनेक गांव पूरी तरह डूबने से बच गए थे। बाद में पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट में लिखा कि बाढ़ के दबाव से ही लाइन कट गई थी।
इन सब दुखद प्रसंगों से राजेंद्र बाबू ने देखा था कि बाढ़ और अकाल अकेले नहीं आते। इनसे पहले समाज में और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए। यह सब कभी धीरे-धीरे, तो कभी बड़ी तेजी से होता है। गति जो भी हो, समाज के नीति निर्धारकों, संचालकों और नेतृत्व का ध्यान इन बातों की तरफ जा नहीं पाता और फिर बाढ़ या अकाल सामने आ खड़ा हो जाता है। बुरे कामों की बाढ़ आ जाती है। बिना पानी का स्वभाव समझे विकास के नाम पर कई तरह के काम होते रहते हैं। यह किसी एक कालखंड की बात नहीं है। दुर्भाग्य से सब समय में ऐसी गलतियां दुहराई जाती रहती हैं। एक तरफ प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ ले जाने वाले कामों की बाढ़ आ जाती है तो दूसरी तरफ अच्छे कामों का अकाल पड़ने लगता है। अच्छे विचारों का अकाल पड़ने लगता है।
राजेंद्र बाबू के जमाने में इन इलाकों में अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों या कहें अनीतियों के कारण बड़ी तेजी से रेल की लाइनें बिछाई गई थी। रेल लाइन उनके व्यापार और शासन के लिए बड़ी खास चीज बन गई थी। इसलिए उसे आसपास की जमीन से ऊंचा उठाकर रखना जरूरी था। आज लोग इस बात को भूल चूके हैं कि कभी हमारे देश में फैल रहा रेल व्यवस्था का यह जाल अंग्रेज सरकार के भी हाथों में नहीं था। वह कुछ निजी अंग्रेजी कंपनियों की जेब में था।
खुद राजेंद्र बाबू अपनी आत्मकथा में इस दुखद प्रसंग में लिखते हैं कि “रेल-लाइनों के कारण बाढ़ की भयंकरता बढ़ जाती है। अपने सूबे में पिछले तीस बरसों में, जितनी बड़ी और भयंकर बाढ़ें आई हैं, सबका मुझे काफी अनुभव है। मेरा यह दृढ़ विचार है कि रेलवे लाइन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तथा दूसरी ऊंची सड़कें बाढ़ के कारणों में प्रमुख हैं। यदि इनमें जगह-जगह काफी संख्या में चौड़े पुल बने रहते तो हालत ऐसी न होती पर यहां तो रेल की कंपनियों के मुनाफे पर ही अधिक ध्यान रखा जाता है। उनको पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, लाइन काटना तो दूर की बात है। बी.एन.डब्ल्यू. रेलवे ने इस मामले में बहुत कंजूसपन दिखलाया है। यद्यपि अब उसमें कई जगह पुल बने हैं, तथापि अब भी बहुत से ऐसे स्थान हैं, जहां पुल की जरूरत है। उसने जो पुल बनवाएं हैं, वे जनता के कष्ट दूर करने के ख्याल से नहीं अपने मुनाफे के ख्याल से, क्योंकि जब तक केवल जनता के कष्ट की बात रही, एक न सुनी गई, पर जब प्रकृति ने लाइन को इस तरह तोड़ा कि महीनों रेल चलना बंद हो गया तो मजबूरन कई पुल बनवा दिए।”
आज हम देखते हैं कि जननीतियां बनाई जाने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। समाज अपना एक जलदर्शन बनाता था और उसे कागज पर न छाप कर लोगों के मन में उकेर देता था। समाज के सदस्य उसे अपने जीवन की रीत बना लेते थे। फिर यह रीत आसानी से टूटती नहीं थी। जलनीतियां आती-जाती सरकारों के साथ बनती-बिगड़ती रहती हैं। पर जल दर्शन बदलता नहीं। इसी रीत से उस क्षेत्र विशेष की फसलें किसान समाज तय कर लेता था। सिंचाई के लिए अपने साधन जुटा लेता था।
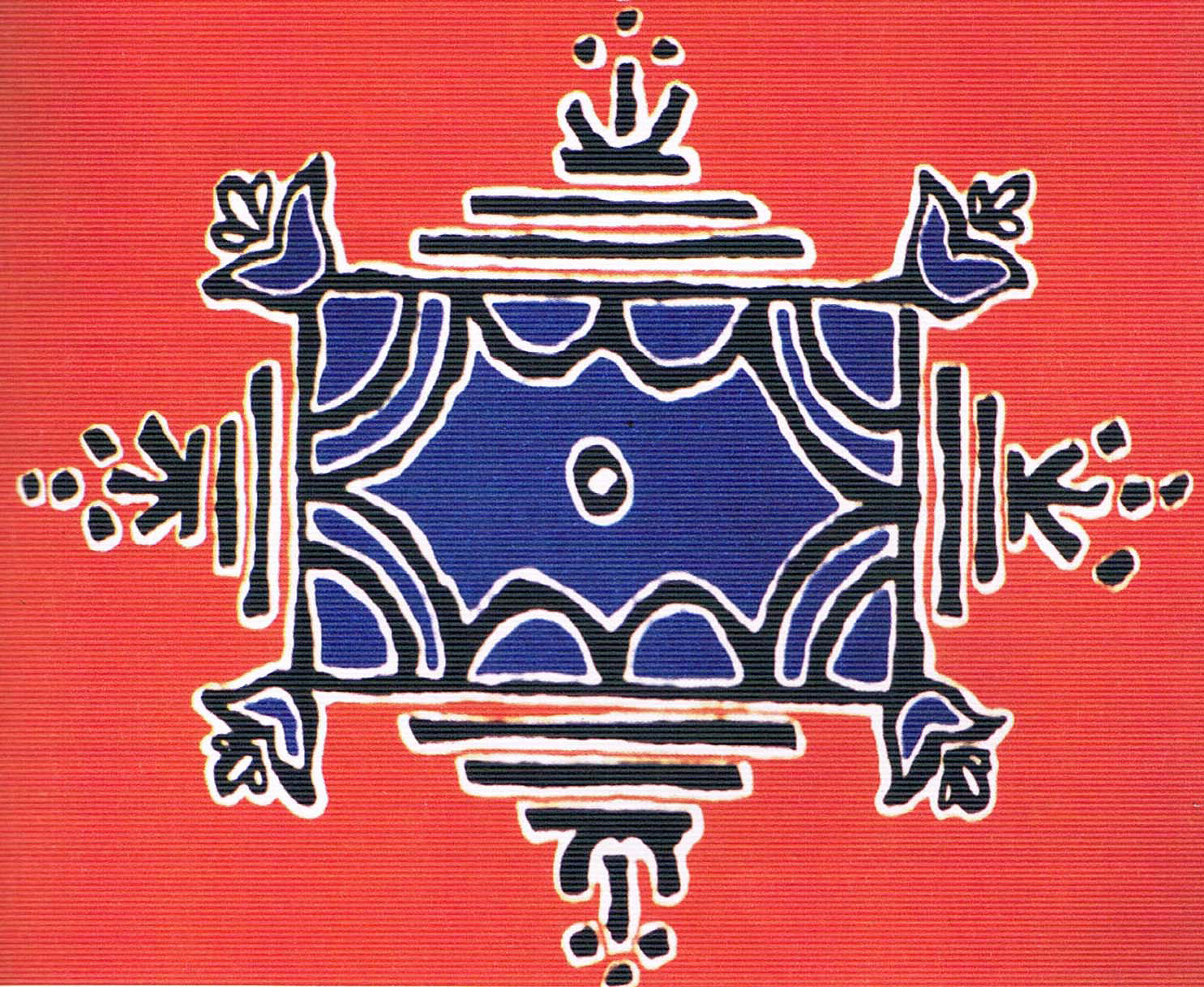 जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था। कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी वैसी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, महाविद्यालय तक नहीं था। सिंचाई की शिक्षा नहीं थी पर सिंचाई का शिक्षण हर जगह था और समाज उस शिक्षण को अपने मन में संजोकर रखता था और उस शिक्षण को अपनी जमीन पर उतारता था। अब अंग्रेज यहां आए हैं- एक बार फिर दुहरा लें तब हमारे यहां एक भी सिविल इंजीनियर नहीं था पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक पश्चिम से पूरब तक कोई 25 लाख छोटे-बड़े तालाब थे। इनसे भी ज्यादा संख्या में जमीन का स्वभाव देखकर अनगिनत कुएं बनाए गए थे। वर्षा का पानी तालाबों में कैसे आएगा, किस तरह के क्षेत्र से, यहां-वहां से बहता आएगा- उसका आगौर अनुभवी आंखों से नाप लिया जाता था। फिर यह पानी साल भर कैसे पीने का पानी जुटाएगा और किस तरह की फसलों को जीवन देगा- इस सबकी बारीक योजना कहीं सैकड़ों मील दूर बैठे लोग नहीं बनाते थे- वहीं बसे लोग उस क्षेत्र में अपना बसना सार्थक करते थे। यह पंरपरा आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है, हां उसकी प्रतिष्ठा जरूर गिर गई है, नए पढ़े-लिखे समाज के मन में।
जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था। कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी वैसी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, महाविद्यालय तक नहीं था। सिंचाई की शिक्षा नहीं थी पर सिंचाई का शिक्षण हर जगह था और समाज उस शिक्षण को अपने मन में संजोकर रखता था और उस शिक्षण को अपनी जमीन पर उतारता था। अब अंग्रेज यहां आए हैं- एक बार फिर दुहरा लें तब हमारे यहां एक भी सिविल इंजीनियर नहीं था पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक पश्चिम से पूरब तक कोई 25 लाख छोटे-बड़े तालाब थे। इनसे भी ज्यादा संख्या में जमीन का स्वभाव देखकर अनगिनत कुएं बनाए गए थे। वर्षा का पानी तालाबों में कैसे आएगा, किस तरह के क्षेत्र से, यहां-वहां से बहता आएगा- उसका आगौर अनुभवी आंखों से नाप लिया जाता था। फिर यह पानी साल भर कैसे पीने का पानी जुटाएगा और किस तरह की फसलों को जीवन देगा- इस सबकी बारीक योजना कहीं सैकड़ों मील दूर बैठे लोग नहीं बनाते थे- वहीं बसे लोग उस क्षेत्र में अपना बसना सार्थक करते थे। यह पंरपरा आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है, हां उसकी प्रतिष्ठा जरूर गिर गई है, नए पढ़े-लिखे समाज के मन में।
पर हमारे इस पढ़े-लिखे समाज को आज यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश की तकनीकी शिक्षा, सिविल इंजीनियरिंग की सारी आधुनिक शिक्षा की नींव में ये अनपढ़ माना गया, अनपढ़ बता दिया गया समाज ही प्रमुख था।
देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था हरिद्वार के पास रूड़की नाम के एक छोटे-से गांव में और सन् था 1847। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ब्रितानी सरकार भी नहीं आई थी। कंपनी का घोषित लक्ष्य देश में व्यापार था। प्रशासन, या लोक कल्याण नहीं। कंपनी तो लूटने के लिए ही बनी थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी देश में उच्च शिक्षा के झंडे भला क्यों गाड़ती।
उस दौर में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह भाग एक भयानक अकाल से गुजर रहा था। अकाल का एक कारण था वर्षा का कम होना। पर अच्छे कामों और अच्छे विचारों का अकाल पहले ही आ चुका था और इसके पीछे एक बड़ा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की अनीतियां।
सौभाग्य से उस क्षेत्र में, तब उसे नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेस कहा जाता था, एक बड़े ही सहृदय अंग्रेज अधिकारी काम कर रहे थे। ऊंचे पद पर थे। वे वहां के उपराज्यपाल थे। नाम था उनका जेम्स थॉमसन। लोगों को अकाल में मरते देख उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को एक पत्र लिख इस क्षेत्र में एक बड़ी नहर को बनाने का प्रस्ताव रखा था। ऊपर से उस पत्र का कोई जवाब तक नहीं आया। थॉमसन ने फिर एक पत्र लिखा। इस बार फिर वही हुआ। कोई जवाब नहीं।
तब जेम्स थॉमसन ने तीसरे पत्र में अपनी योजना में पानी और अकाल, लोगों के कष्टों के बदले व्यापार की, मुनाफे की चमक डाली। उन्होंने हिसाब लिखा कि इसमें इतने रुपए लगाने से इतने ज्यादा रुपए सिंचाई के कर की तरह मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में चमक आ गई। मुनाफा मिलेगा तो ठीक। बनाओ। पर बनाएगा कौन? कोई इंजीनियर तो है नहीं कंपनी के पास। थॉमसन ने कंपनी को आश्वस्त किया था कि यहां गांवों के लोग इसे बना लेंगे।
कोई ऐरी-गैरी, छोटी-मोटी योजना नहीं थी यह। हरिद्वार के पास गंगा से एक नहर निकाल कर उसे कोई 200 किलोमीटर तक के इलाके में फैलाना था। यह न सिर्फ अपने देश की एक पहली बड़ी सिंचाई योजना थी, दुनिया के कई अन्य देशों में भी उस समय ऐसा कोई काम हुआ नहीं था।
वह योजना खूब अच्छे ढंग से पूरी हुई। तब थॉमसन ने कंपनी से इसकी सफलता को देखते हुए इस क्षेत्र में इसी नहर के किनारे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव रखा। इसे भी मान लिया गया क्योंकि थॉमसन ने इस प्रस्ताव में भी बड़ी कुशलता से कंपनी को याद दिलाया था कि इस कॉलेज से निकले छात्र बाद में आपके साम्राज्य का विस्तार करने में मददगार होंगे।
यह था सन् 1847 में बना देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। देश का ही नहीं, एशिया का भी यह पहला कॉलेज था, इस विषय को पढ़ाने वाला। तब इंग्लैंड में भी इस तरह का कोई कॉलेज नहीं था। रुड़की के इस कॉलेज में कुछ साल बाद इंग्लैंड से भी छात्रों का एक दल यहां पढ़ने के लिए भेजा गया था।
तो इस कॉलेज की नींव में हमारा अनपढ़ बता दिया गया समाज मजबूती से सिर उठाए खड़ा है। वह तब भी नहीं दिखा था अन्य लोगों को और आज तो हम उसे पिछड़ा बता कर उसके विकास की बहुविध कोशिश में लगे हैं। इस प्रसंग के अंत में यह भी बता देना चाहिए कि 1847 में कॉलेज खुलने से पहले वहां बनी वह लंबी नहर आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों में गंगा का पानी सिंचाई के लिए वितरित करती जा रही है। आज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को शासन ने और ऊंचा दर्जा देकर उसे आईआईटी रुड़की बना दिया है।
कॉलेज का दर्जा तो उठा है पर दुर्भाग्य से कॉलेज जिन लोगों के कारण बना, जिनके कारण वह विशाल सिंचाई योजना जमीन पर उतरी, जिन लोगों ने अंग्रेजों के आने से पहले देश में, देश के मैदानी भागों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, देश के तटवर्ती क्षेत्रों में जल दर्शन का सुंदर संयोजन किया था, वे लोग आज कहीं पीछे फेंक दिए गए हैं।
 हमारे देश की समुद्र तटीय रेखा बहुत बड़ी है। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी घूमते हुए यह रेखा बंगाल में सुंदरवन तक एक बड़ा भाग घूम लेती है। पश्चिमी तट पर बहुत कम लेकिन पूर्वी तट पर अब समुद्री तूफानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता भी बढ़ती रही है।
हमारे देश की समुद्र तटीय रेखा बहुत बड़ी है। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी घूमते हुए यह रेखा बंगाल में सुंदरवन तक एक बड़ा भाग घूम लेती है। पश्चिमी तट पर बहुत कम लेकिन पूर्वी तट पर अब समुद्री तूफानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता भी बढ़ती रही है।
इसके पीछे एक बड़ा कारण है हमारे कुल तटीय प्रदेशों में उन विशेष वनों का लगातार कटते जाना, जिनके कारण ऐसे तूफान तट पर टकराते समय विध्वंस की अपनी ताकत काफी कुछ खो देते थे।
समुद्र और धरती के मिलन बिंदु पर, हजारों वर्षों से एक उत्सव की तरह खड़े ये वन बहुत ही विशिष्ट स्वभाव लिए होते हैं। दिन में दो बार ये खारे पानी में डूबते हैं तो दो बार पीछे से आ रही नदी के मीठे पानी में। मैदान, पहाड़ों में लगे पेड़ों से, वनों से इनकी तुलना करना ठीक नहीं। वनस्पति का ऐसा दर्शन अन्य किसी स्थान पर संभव नहीं। यहां इन पेड़ों की, वनों की जड़ें भी ऊपर रहती हैं। अंधेरे में, मिट्टी के भीतर नहीं, प्रकाश में, मिट्टी के ऊपर। जड़ें, तना और फिर शाखाएं-तीनों का दर्शन एक साथ करा देने वाला यह वृक्ष, उसका पूरा वन इतना सुंदर होता है कि इस प्रजाति का एक नाम हमारे देश में सुंदर, सुंदरी ही रखा दिया गया था। उसी से बना है सुंदरवन।
लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारा पढ़ा-लिखा संसार, हमारे वैज्ञानिक कोई 13-14 प्रदेशों में फैले इस वन के, इस प्रजाति के अपने नाम एकदम भूल गए हैं। जब भी इन वनों की चर्चा होती है, इन्हें इनके अंग्रेजी ‘मैंग्रोव’- से ही जाना जाता है। हमारे ध्यान में भी यह बात नहीं आ पाती कि देश में, कम से कम इन प्रदेशों की भाषाओं में, बोलियों में तो इन वनों का नाम होगा। उसके गुणों की स्मृति होगी।
तटीय प्रदेशों से प्रारंभ करें तो पश्चिम में ऊपर गुजराती व कच्छी में इसे चैरव, फिर मराठी में कोंकणी में खार पुटी, तिवर, कन्नड़ में कांडला काडु, तमिल में सधुप्पू निल्लम काड्ड, तेलुगू में माडा आडवी, उड़िया में झाऊवन कहा जाता है। बांग्ला में तो सुंदरवन सबने सुना ही है। एक नाम मकड़सिरा भी है और हिन्दी प्रदेश तो समुद्र के तट से दूर ही हैं पर ऐसा नहीं होता कि जो चीज जिस समाज में नहीं है, उस समाज की भाषा उसका नाम ही नहीं रखे। हिन्दी में इसे चमरंग वन कहते थे। पर अब यह नए शब्दकोशों से बाहर हो गया है।
पर्यावरण को ठीक से जानने वाले बताते हैं कि आंध्र और उड़िया में खासकर पाराद्वीप वाले भाग में चमरंग वनों को विकास के नाम पर खूब ही उजाड़ा है। इसीलिए पाराद्वीप ऐसे ही एक चक्रवात में बुरी तरह से नष्ट हुआ था। फिर यह भी कहा गया था कि उसके लिए एक मजबूत दीवार बना दी जाएगी। कुछ ठंडे देशों का अपवाद छोड़ दें तो पूरी दुनिया में धरती और समुद्र के मिलने की जगह पर प्रकृति ने सुरक्षा के ख्याल से ही यह हरी सुंदर दीवार, लंबे-चौड़े सुंदरवन खड़े किए थे। आज हम अपने लालच में इन्हें काट कर इनके बदले पांच गज चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की दीवार खड़ी कर सुरक्षित रह जाएंगे- ऐसा सोचना कितनी मूर्खता होगी। चौथी की कक्षाओं में यह पढ़ा दिया जाता है कि पृथ्वी पर कोई सत्तर प्रतिशत भाग में समुद्र है और धरती बस तीस प्रतिशत ही है। समुद्र के सामने हम नगण्य हैं। ये सुंदरवन, चमरंग वन हमारी गिनती बनी रहे- ऐसी सुरक्षा देते हैं।
दीवारें खड़ी करने से समुद्र पीछे हट जाएगा, तटबंध बना देने से बाढ़ रुक जाएगी, बाहर से अनाज मंगवाकर बांट देने से अकाल दूर हो जाएगा- बुरे विचारों की ऐसी बाढ़ से, अच्छे विचारों के ऐसे ही अकाल से हमारा यह जल संकट बढ़ा है।
अश्विन के महीने में बिहार के छपरा जिले में एक दिन घनघोर बरसात हुई। चौबीस घंटों में लगभग छत्तीस इंच वर्षा हुई, नतीजा यह हुआ कि पूरा जिला भयानक बाढ़ में डूब गया। वहां के सरकारी कर्मचारियों ने लोगों की इस मुसीबत में बहुत ही उदासीनता और उपेक्षा का भाव दिखाया। उन दिनों छपरा से मशरक तक जाने वाली रेल लाइन के कारण बाढ़ का सारा पानी आगे बहने के बदले एक बड़े भाग में फैल गया था और पीछे से आने वाली विशाल धारा उसका स्तर लगातार उठाते जा रही थी। लोगों को इससे बचने का एक ही रास्ता दिखा था, रेलवे लाइन काट देना और चढ़ते पानी को आगे के भूभाग में फैलने देना जहां कुछ सांस ली जा सके। पर कलेक्टर ने उनकी एक न सुनी और तो और ऐसी ही तबाही मचा रही अन्य रेलवे लाइनों पर सशस्त्र पहरा बिठा दिया गया था। सीवान के पास एक ऐसी ही जगह बहुत पानी जमा हो गया था। गांव वालों ने तब खुद ही उस रेल लाइन को काटना तय कर लिया। पर सामने सशस्त्र पुलिस देख उनकी हिम्मत न पड़ी।
राजेंद्र बाबू इसका वर्णन करते हुए लिखते हैः “कष्ट सहते गए लोग। पर जब वह बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दो-चार आदमी कंधे पर कुदाल रखकर पानी में तैरते हुए रेल लाइन की तरफ बढ़े। पुलिस ने उन्हें देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब दिया कि पानी में डूब कर तो हम मर ही रहे हैं और तुम लाइन नहीं काटने देते। अब तक हमने बर्दाश्त किया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरना दोनों हालत में है। डूब कर मरें या गोली खाकर मरें। हमने निश्चय कर लिया है कि गोली खाकर मरना बेहतर है। हम लाइन काटेंगे, तुम गोली मारो।”
बहते पानी में ये बहादुर लोग तैरते हुए मजबूत बांध की तरह उठी हुई उस रेल लाइन पर अपने दृढ़-निश्चय से कुदाल चलाते गए। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई गोली चलाने की। लाइन अभी थोड़ी-सी ही कट पाई थी कि पीछे भर रहे पानी की ताकत ने लोगों के संकल्प में साथ दिया और लाइन भड़ाक से टूटी और विशाल बाढ़ का पानी उसे किसी तिनके की तरह अपने साथ न जाने कहां बहा ले गया। पीछे के अनेक गांव पूरी तरह डूबने से बच गए थे। बाद में पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट में लिखा कि बाढ़ के दबाव से ही लाइन कट गई थी।
इन सब दुखद प्रसंगों से राजेंद्र बाबू ने देखा था कि बाढ़ और अकाल अकेले नहीं आते। इनसे पहले समाज में और भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए। यह सब कभी धीरे-धीरे, तो कभी बड़ी तेजी से होता है। गति जो भी हो, समाज के नीति निर्धारकों, संचालकों और नेतृत्व का ध्यान इन बातों की तरफ जा नहीं पाता और फिर बाढ़ या अकाल सामने आ खड़ा हो जाता है। बुरे कामों की बाढ़ आ जाती है। बिना पानी का स्वभाव समझे विकास के नाम पर कई तरह के काम होते रहते हैं। यह किसी एक कालखंड की बात नहीं है। दुर्भाग्य से सब समय में ऐसी गलतियां दुहराई जाती रहती हैं। एक तरफ प्रकृति और पर्यावरण के खिलाफ ले जाने वाले कामों की बाढ़ आ जाती है तो दूसरी तरफ अच्छे कामों का अकाल पड़ने लगता है। अच्छे विचारों का अकाल पड़ने लगता है।
राजेंद्र बाबू के जमाने में इन इलाकों में अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों या कहें अनीतियों के कारण बड़ी तेजी से रेल की लाइनें बिछाई गई थी। रेल लाइन उनके व्यापार और शासन के लिए बड़ी खास चीज बन गई थी। इसलिए उसे आसपास की जमीन से ऊंचा उठाकर रखना जरूरी था। आज लोग इस बात को भूल चूके हैं कि कभी हमारे देश में फैल रहा रेल व्यवस्था का यह जाल अंग्रेज सरकार के भी हाथों में नहीं था। वह कुछ निजी अंग्रेजी कंपनियों की जेब में था।
खुद राजेंद्र बाबू अपनी आत्मकथा में इस दुखद प्रसंग में लिखते हैं कि “रेल-लाइनों के कारण बाढ़ की भयंकरता बढ़ जाती है। अपने सूबे में पिछले तीस बरसों में, जितनी बड़ी और भयंकर बाढ़ें आई हैं, सबका मुझे काफी अनुभव है। मेरा यह दृढ़ विचार है कि रेलवे लाइन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तथा दूसरी ऊंची सड़कें बाढ़ के कारणों में प्रमुख हैं। यदि इनमें जगह-जगह काफी संख्या में चौड़े पुल बने रहते तो हालत ऐसी न होती पर यहां तो रेल की कंपनियों के मुनाफे पर ही अधिक ध्यान रखा जाता है। उनको पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, लाइन काटना तो दूर की बात है। बी.एन.डब्ल्यू. रेलवे ने इस मामले में बहुत कंजूसपन दिखलाया है। यद्यपि अब उसमें कई जगह पुल बने हैं, तथापि अब भी बहुत से ऐसे स्थान हैं, जहां पुल की जरूरत है। उसने जो पुल बनवाएं हैं, वे जनता के कष्ट दूर करने के ख्याल से नहीं अपने मुनाफे के ख्याल से, क्योंकि जब तक केवल जनता के कष्ट की बात रही, एक न सुनी गई, पर जब प्रकृति ने लाइन को इस तरह तोड़ा कि महीनों रेल चलना बंद हो गया तो मजबूरन कई पुल बनवा दिए।”
गंगा नहर और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज
आज हम देखते हैं कि जननीतियां बनाई जाने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। समाज अपना एक जलदर्शन बनाता था और उसे कागज पर न छाप कर लोगों के मन में उकेर देता था। समाज के सदस्य उसे अपने जीवन की रीत बना लेते थे। फिर यह रीत आसानी से टूटती नहीं थी। जलनीतियां आती-जाती सरकारों के साथ बनती-बिगड़ती रहती हैं। पर जल दर्शन बदलता नहीं। इसी रीत से उस क्षेत्र विशेष की फसलें किसान समाज तय कर लेता था। सिंचाई के लिए अपने साधन जुटा लेता था।
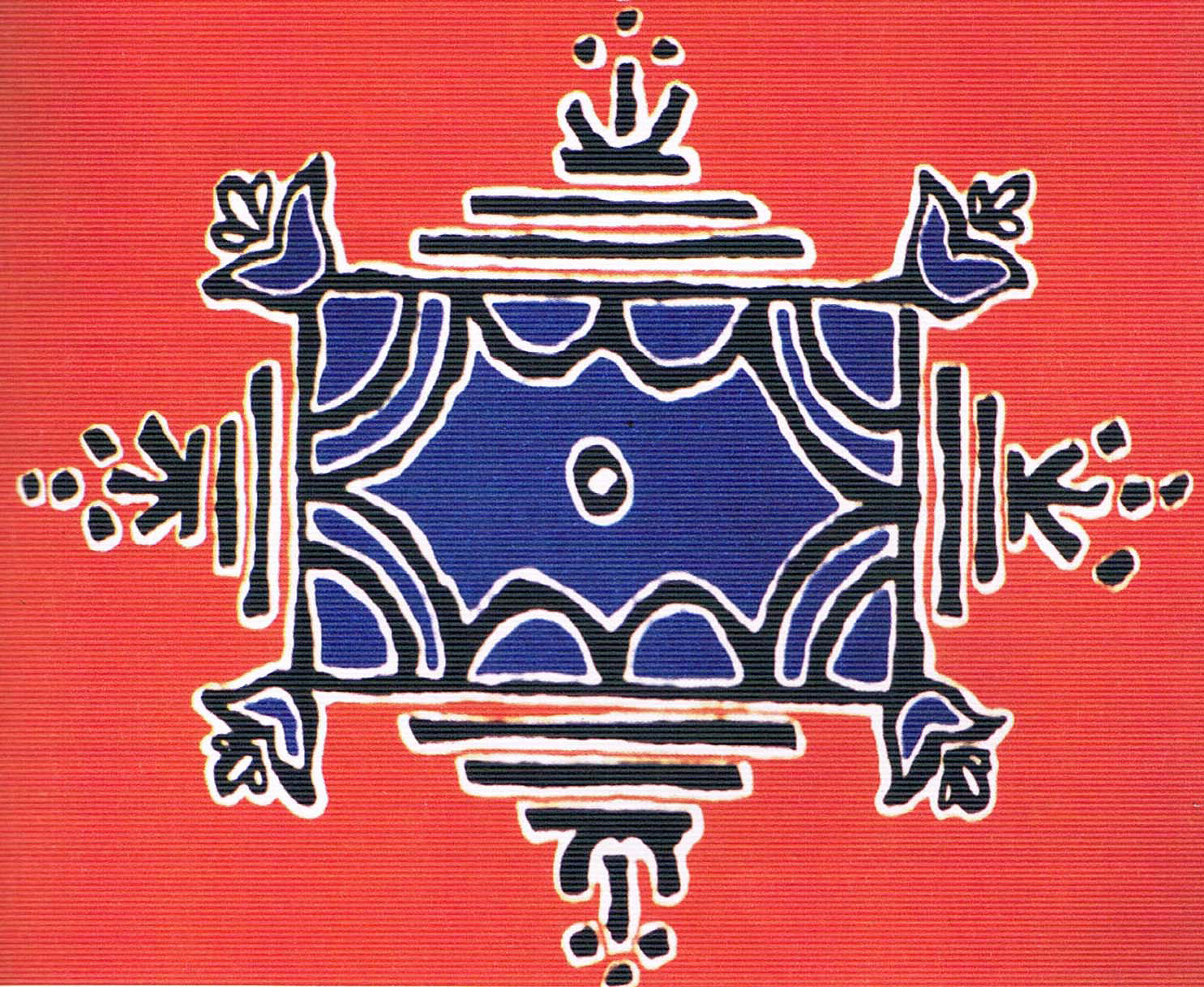 जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था। कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी वैसी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, महाविद्यालय तक नहीं था। सिंचाई की शिक्षा नहीं थी पर सिंचाई का शिक्षण हर जगह था और समाज उस शिक्षण को अपने मन में संजोकर रखता था और उस शिक्षण को अपनी जमीन पर उतारता था। अब अंग्रेज यहां आए हैं- एक बार फिर दुहरा लें तब हमारे यहां एक भी सिविल इंजीनियर नहीं था पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक पश्चिम से पूरब तक कोई 25 लाख छोटे-बड़े तालाब थे। इनसे भी ज्यादा संख्या में जमीन का स्वभाव देखकर अनगिनत कुएं बनाए गए थे। वर्षा का पानी तालाबों में कैसे आएगा, किस तरह के क्षेत्र से, यहां-वहां से बहता आएगा- उसका आगौर अनुभवी आंखों से नाप लिया जाता था। फिर यह पानी साल भर कैसे पीने का पानी जुटाएगा और किस तरह की फसलों को जीवन देगा- इस सबकी बारीक योजना कहीं सैकड़ों मील दूर बैठे लोग नहीं बनाते थे- वहीं बसे लोग उस क्षेत्र में अपना बसना सार्थक करते थे। यह पंरपरा आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है, हां उसकी प्रतिष्ठा जरूर गिर गई है, नए पढ़े-लिखे समाज के मन में।
जब अंग्रेज हमारे यहां आए थे तो हमारे देश में कोई सिंचाई विभाग नहीं था। कोई इंजीनियर नहीं था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं थी वैसी शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय, महाविद्यालय तक नहीं था। सिंचाई की शिक्षा नहीं थी पर सिंचाई का शिक्षण हर जगह था और समाज उस शिक्षण को अपने मन में संजोकर रखता था और उस शिक्षण को अपनी जमीन पर उतारता था। अब अंग्रेज यहां आए हैं- एक बार फिर दुहरा लें तब हमारे यहां एक भी सिविल इंजीनियर नहीं था पर सचमुच कश्मीर से कन्याकुमारी तक पश्चिम से पूरब तक कोई 25 लाख छोटे-बड़े तालाब थे। इनसे भी ज्यादा संख्या में जमीन का स्वभाव देखकर अनगिनत कुएं बनाए गए थे। वर्षा का पानी तालाबों में कैसे आएगा, किस तरह के क्षेत्र से, यहां-वहां से बहता आएगा- उसका आगौर अनुभवी आंखों से नाप लिया जाता था। फिर यह पानी साल भर कैसे पीने का पानी जुटाएगा और किस तरह की फसलों को जीवन देगा- इस सबकी बारीक योजना कहीं सैकड़ों मील दूर बैठे लोग नहीं बनाते थे- वहीं बसे लोग उस क्षेत्र में अपना बसना सार्थक करते थे। यह पंरपरा आज भी पूरी तरह से टूटी नहीं है, हां उसकी प्रतिष्ठा जरूर गिर गई है, नए पढ़े-लिखे समाज के मन में।पर हमारे इस पढ़े-लिखे समाज को आज यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश की तकनीकी शिक्षा, सिविल इंजीनियरिंग की सारी आधुनिक शिक्षा की नींव में ये अनपढ़ माना गया, अनपढ़ बता दिया गया समाज ही प्रमुख था।
देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था हरिद्वार के पास रूड़की नाम के एक छोटे-से गांव में और सन् था 1847। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ब्रितानी सरकार भी नहीं आई थी। कंपनी का घोषित लक्ष्य देश में व्यापार था। प्रशासन, या लोक कल्याण नहीं। कंपनी तो लूटने के लिए ही बनी थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी देश में उच्च शिक्षा के झंडे भला क्यों गाड़ती।
उस दौर में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह भाग एक भयानक अकाल से गुजर रहा था। अकाल का एक कारण था वर्षा का कम होना। पर अच्छे कामों और अच्छे विचारों का अकाल पहले ही आ चुका था और इसके पीछे एक बड़ा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की अनीतियां।
सौभाग्य से उस क्षेत्र में, तब उसे नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेस कहा जाता था, एक बड़े ही सहृदय अंग्रेज अधिकारी काम कर रहे थे। ऊंचे पद पर थे। वे वहां के उपराज्यपाल थे। नाम था उनका जेम्स थॉमसन। लोगों को अकाल में मरते देख उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को एक पत्र लिख इस क्षेत्र में एक बड़ी नहर को बनाने का प्रस्ताव रखा था। ऊपर से उस पत्र का कोई जवाब तक नहीं आया। थॉमसन ने फिर एक पत्र लिखा। इस बार फिर वही हुआ। कोई जवाब नहीं।
तब जेम्स थॉमसन ने तीसरे पत्र में अपनी योजना में पानी और अकाल, लोगों के कष्टों के बदले व्यापार की, मुनाफे की चमक डाली। उन्होंने हिसाब लिखा कि इसमें इतने रुपए लगाने से इतने ज्यादा रुपए सिंचाई के कर की तरह मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में चमक आ गई। मुनाफा मिलेगा तो ठीक। बनाओ। पर बनाएगा कौन? कोई इंजीनियर तो है नहीं कंपनी के पास। थॉमसन ने कंपनी को आश्वस्त किया था कि यहां गांवों के लोग इसे बना लेंगे।
कोई ऐरी-गैरी, छोटी-मोटी योजना नहीं थी यह। हरिद्वार के पास गंगा से एक नहर निकाल कर उसे कोई 200 किलोमीटर तक के इलाके में फैलाना था। यह न सिर्फ अपने देश की एक पहली बड़ी सिंचाई योजना थी, दुनिया के कई अन्य देशों में भी उस समय ऐसा कोई काम हुआ नहीं था।
वह योजना खूब अच्छे ढंग से पूरी हुई। तब थॉमसन ने कंपनी से इसकी सफलता को देखते हुए इस क्षेत्र में इसी नहर के किनारे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव रखा। इसे भी मान लिया गया क्योंकि थॉमसन ने इस प्रस्ताव में भी बड़ी कुशलता से कंपनी को याद दिलाया था कि इस कॉलेज से निकले छात्र बाद में आपके साम्राज्य का विस्तार करने में मददगार होंगे।
यह था सन् 1847 में बना देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। देश का ही नहीं, एशिया का भी यह पहला कॉलेज था, इस विषय को पढ़ाने वाला। तब इंग्लैंड में भी इस तरह का कोई कॉलेज नहीं था। रुड़की के इस कॉलेज में कुछ साल बाद इंग्लैंड से भी छात्रों का एक दल यहां पढ़ने के लिए भेजा गया था।
तो इस कॉलेज की नींव में हमारा अनपढ़ बता दिया गया समाज मजबूती से सिर उठाए खड़ा है। वह तब भी नहीं दिखा था अन्य लोगों को और आज तो हम उसे पिछड़ा बता कर उसके विकास की बहुविध कोशिश में लगे हैं। इस प्रसंग के अंत में यह भी बता देना चाहिए कि 1847 में कॉलेज खुलने से पहले वहां बनी वह लंबी नहर आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेतों में गंगा का पानी सिंचाई के लिए वितरित करती जा रही है। आज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को शासन ने और ऊंचा दर्जा देकर उसे आईआईटी रुड़की बना दिया है।
कॉलेज का दर्जा तो उठा है पर दुर्भाग्य से कॉलेज जिन लोगों के कारण बना, जिनके कारण वह विशाल सिंचाई योजना जमीन पर उतरी, जिन लोगों ने अंग्रेजों के आने से पहले देश में, देश के मैदानी भागों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, देश के तटवर्ती क्षेत्रों में जल दर्शन का सुंदर संयोजन किया था, वे लोग आज कहीं पीछे फेंक दिए गए हैं।
तूफान और तटीय जंगल
 हमारे देश की समुद्र तटीय रेखा बहुत बड़ी है। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी घूमते हुए यह रेखा बंगाल में सुंदरवन तक एक बड़ा भाग घूम लेती है। पश्चिमी तट पर बहुत कम लेकिन पूर्वी तट पर अब समुद्री तूफानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता भी बढ़ती रही है।
हमारे देश की समुद्र तटीय रेखा बहुत बड़ी है। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी घूमते हुए यह रेखा बंगाल में सुंदरवन तक एक बड़ा भाग घूम लेती है। पश्चिमी तट पर बहुत कम लेकिन पूर्वी तट पर अब समुद्री तूफानों की संख्या और उनकी मारक क्षमता भी बढ़ती रही है।इसके पीछे एक बड़ा कारण है हमारे कुल तटीय प्रदेशों में उन विशेष वनों का लगातार कटते जाना, जिनके कारण ऐसे तूफान तट पर टकराते समय विध्वंस की अपनी ताकत काफी कुछ खो देते थे।
समुद्र और धरती के मिलन बिंदु पर, हजारों वर्षों से एक उत्सव की तरह खड़े ये वन बहुत ही विशिष्ट स्वभाव लिए होते हैं। दिन में दो बार ये खारे पानी में डूबते हैं तो दो बार पीछे से आ रही नदी के मीठे पानी में। मैदान, पहाड़ों में लगे पेड़ों से, वनों से इनकी तुलना करना ठीक नहीं। वनस्पति का ऐसा दर्शन अन्य किसी स्थान पर संभव नहीं। यहां इन पेड़ों की, वनों की जड़ें भी ऊपर रहती हैं। अंधेरे में, मिट्टी के भीतर नहीं, प्रकाश में, मिट्टी के ऊपर। जड़ें, तना और फिर शाखाएं-तीनों का दर्शन एक साथ करा देने वाला यह वृक्ष, उसका पूरा वन इतना सुंदर होता है कि इस प्रजाति का एक नाम हमारे देश में सुंदर, सुंदरी ही रखा दिया गया था। उसी से बना है सुंदरवन।
लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारा पढ़ा-लिखा संसार, हमारे वैज्ञानिक कोई 13-14 प्रदेशों में फैले इस वन के, इस प्रजाति के अपने नाम एकदम भूल गए हैं। जब भी इन वनों की चर्चा होती है, इन्हें इनके अंग्रेजी ‘मैंग्रोव’- से ही जाना जाता है। हमारे ध्यान में भी यह बात नहीं आ पाती कि देश में, कम से कम इन प्रदेशों की भाषाओं में, बोलियों में तो इन वनों का नाम होगा। उसके गुणों की स्मृति होगी।
तटीय प्रदेशों से प्रारंभ करें तो पश्चिम में ऊपर गुजराती व कच्छी में इसे चैरव, फिर मराठी में कोंकणी में खार पुटी, तिवर, कन्नड़ में कांडला काडु, तमिल में सधुप्पू निल्लम काड्ड, तेलुगू में माडा आडवी, उड़िया में झाऊवन कहा जाता है। बांग्ला में तो सुंदरवन सबने सुना ही है। एक नाम मकड़सिरा भी है और हिन्दी प्रदेश तो समुद्र के तट से दूर ही हैं पर ऐसा नहीं होता कि जो चीज जिस समाज में नहीं है, उस समाज की भाषा उसका नाम ही नहीं रखे। हिन्दी में इसे चमरंग वन कहते थे। पर अब यह नए शब्दकोशों से बाहर हो गया है।
पर्यावरण को ठीक से जानने वाले बताते हैं कि आंध्र और उड़िया में खासकर पाराद्वीप वाले भाग में चमरंग वनों को विकास के नाम पर खूब ही उजाड़ा है। इसीलिए पाराद्वीप ऐसे ही एक चक्रवात में बुरी तरह से नष्ट हुआ था। फिर यह भी कहा गया था कि उसके लिए एक मजबूत दीवार बना दी जाएगी। कुछ ठंडे देशों का अपवाद छोड़ दें तो पूरी दुनिया में धरती और समुद्र के मिलने की जगह पर प्रकृति ने सुरक्षा के ख्याल से ही यह हरी सुंदर दीवार, लंबे-चौड़े सुंदरवन खड़े किए थे। आज हम अपने लालच में इन्हें काट कर इनके बदले पांच गज चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की दीवार खड़ी कर सुरक्षित रह जाएंगे- ऐसा सोचना कितनी मूर्खता होगी। चौथी की कक्षाओं में यह पढ़ा दिया जाता है कि पृथ्वी पर कोई सत्तर प्रतिशत भाग में समुद्र है और धरती बस तीस प्रतिशत ही है। समुद्र के सामने हम नगण्य हैं। ये सुंदरवन, चमरंग वन हमारी गिनती बनी रहे- ऐसी सुरक्षा देते हैं।
दीवारें खड़ी करने से समुद्र पीछे हट जाएगा, तटबंध बना देने से बाढ़ रुक जाएगी, बाहर से अनाज मंगवाकर बांट देने से अकाल दूर हो जाएगा- बुरे विचारों की ऐसी बाढ़ से, अच्छे विचारों के ऐसे ही अकाल से हमारा यह जल संकट बढ़ा है।
Path Alias
/articles/barabaadai-kai-baadha-samajha-kaa-akaala
Post By: admin