सरकार को बुन्देलखण्ड में सूखे की समस्या से निपटने के लिये पुराने तालाबों व अन्य जल संग्रह माध्यमों का पुनरुद्धार करना चाहिए था लेकिन उसने नए जल संरक्षण ढाँचे बनाने में ही 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
 मानवती (38 वर्ष) पिछले दो घंटों से करीब स्थित हैण्डपम्प पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इतनी मेहनत के बाद उनको आधा बाल्टी पानी मिल सका है। थकहार कर वह अपनी पड़ोसी कपूरी के साथ वहाँ से एक दूसरे हैण्डपम्प की ओर चल देती हैं जो उनके गाँव सलैया कर्राह से दो किलोमीटर दूर स्थित है। मानवती कहती हैं, “यह गाँव का इकलौता हैण्डपम्प है लेकिन अब यह भी सूख रहा है। मुझे अंधेरा होने से पहले अपने तीनों बच्चों के लिये खाना पकाना है क्योंकि शाम साढ़े छह बजे बिजली कट जाएगी तो रात भर नहीं आएगी।” शाम के साढ़े पाँच बज चुके हैं और उनके पास पानी लाने के लिये केवल एक घंटे का वक्त बचा है।
मानवती (38 वर्ष) पिछले दो घंटों से करीब स्थित हैण्डपम्प पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इतनी मेहनत के बाद उनको आधा बाल्टी पानी मिल सका है। थकहार कर वह अपनी पड़ोसी कपूरी के साथ वहाँ से एक दूसरे हैण्डपम्प की ओर चल देती हैं जो उनके गाँव सलैया कर्राह से दो किलोमीटर दूर स्थित है। मानवती कहती हैं, “यह गाँव का इकलौता हैण्डपम्प है लेकिन अब यह भी सूख रहा है। मुझे अंधेरा होने से पहले अपने तीनों बच्चों के लिये खाना पकाना है क्योंकि शाम साढ़े छह बजे बिजली कट जाएगी तो रात भर नहीं आएगी।” शाम के साढ़े पाँच बज चुके हैं और उनके पास पानी लाने के लिये केवल एक घंटे का वक्त बचा है। मानवती मध्य भारत के बुन्देलखण्ड इलाके की अनेक महिलाओं में से एक हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों से मिलकर बने इस इलाके की महिलाओं को पानी के लिये रोज ऐसा ही संघर्ष करना होता है। उनका गाँव उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पड़ता है। यह इलाका हमेशा से पानी की कमी का शिकार रहा है लेकिन पिछले कुछ दशक में यहाँ हालात बद से बदतर हो चले हैं। मानवती का पति महोबा में दैनिक मजदूर का काम करता है। उनके ससुर लाल चतुर्वेदी के पास तीन हेक्टेयर जमीन है लेकिन पिछले दो साल से वहाँ खेती नहीं हो सकी है क्योंकि इसके लिये पर्याप्त पानी नहीं है। उन्होंने तीन साल पहले ट्रैक्टर खरीदने के लिये कर्ज लिया था लेकिन वह पिछले साल से एक लाख रुपये की सालाना किश्त नहीं जमा कर पाए हैं। बैंक ने उनके घर रिकवरी एजेंट भेजने शुरू कर दिए हैं जो बदतमीजी करते हैं। परिवार इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं चतुर्वेदी आत्महत्या न कर लें। आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक जून 2015 से मार्च 2016 के दरमियान 27 किसानों ने आत्महत्या की है।
 पानी की कमी के कारण फसल खराब हुई, दंगे हुए, जातिगत हिंसा भड़की और बहुत बड़े पैमाने पर लोग इलाका छोड़कर बाहर चले गए। उदाहरण के लिये जिले के कबराई ब्लॉक मेंं रहने वाले मनोज बसोर पेशे से सफाई कर्मी हैं। उनको ऊँची जाति के लोगों ने इसलिये पीटा क्योंकि उन्होंने उनका हैण्डपम्प छू दिया था। अपने घाव दिखाते हुए मनोज कहते हैं, “मैं अस्पृश्य जाति का हूँ। मुझे प्यास लगी थी इसलिये मैंने पानी लेने के लिये हैण्डपम्प छू दिया। उन लोगों ने न केवल मुझ पर हमला किया बल्कि पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी।” कबराई पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ-साथ पानी से जुड़े अपराध और बढ़ेंगे। थाने के एक कांस्टेबल राब बहादुर सिंह कहते हैं कि गत वर्ष थाने में ऐसे 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पाँच मामले आ चुके हैं।
पानी की कमी के कारण फसल खराब हुई, दंगे हुए, जातिगत हिंसा भड़की और बहुत बड़े पैमाने पर लोग इलाका छोड़कर बाहर चले गए। उदाहरण के लिये जिले के कबराई ब्लॉक मेंं रहने वाले मनोज बसोर पेशे से सफाई कर्मी हैं। उनको ऊँची जाति के लोगों ने इसलिये पीटा क्योंकि उन्होंने उनका हैण्डपम्प छू दिया था। अपने घाव दिखाते हुए मनोज कहते हैं, “मैं अस्पृश्य जाति का हूँ। मुझे प्यास लगी थी इसलिये मैंने पानी लेने के लिये हैण्डपम्प छू दिया। उन लोगों ने न केवल मुझ पर हमला किया बल्कि पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी।” कबराई पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ-साथ पानी से जुड़े अपराध और बढ़ेंगे। थाने के एक कांस्टेबल राब बहादुर सिंह कहते हैं कि गत वर्ष थाने में ऐसे 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पाँच मामले आ चुके हैं। कबराई में ही रहने वाले एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी यू. एन. तिवारी कहते हैं कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चलती है। पानी के टैंकर आते ही लूट लिये जाते हैं। पिछली बार तिवारी केवल तीन बाल्टी पानी हासिल कर सके थे, वह भी इसलिये क्योंकि पानी पुलिस के संरक्षण में बाँटा गया था। उनको पूरे चार दिन इन तीन बाल्टी पानी के दम पर काटने पड़े। उनकी पत्नी मॉनसून के आने तक अपने बच्चों के पास भोपाल चली गई हैं।
स्थायी संकट
पिछले 15 सालों में बुन्देलखण्ड में 13वीं बार सूखा पड़ा है लेकिन हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक 18वीं और 19वीं सदी में इस क्षेत्र में 16 साल में एक बार सूखा पड़ता था। सन 1968 से 1992 के बीच सूखे की आवृत्ति बढ़ती चली गई। इस अवधि में हर पाँच साल में एक बार सूखा पड़ता गया। वर्ष 2004 और 2008 के बीच लगातार चार बार पड़े सूखे ने इस क्षेत्र को संकट में डाल दिया। वर्ष 2013 को छोड़ दिया जाए तो 2009 से 2015 के बीच हर साल मॉनसून कमजोर रहा है। महोबा स्थित गैर सरकारी संगठन ग्रामोन्नति संस्थान के परियोजना समन्वयक राजेंद्र निगम कहते हैं कि वर्ष 2013 में भी फरवरी में अतिरिक्त वर्षा हुई थी और भारी बारिश ने रबी और खरीफ की 60 फीसदी फसल नष्ट कर दी थी।
 सूखे के कारण लगातार 15वीं बार फसल खराब हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक बुन्देलखण्ड इलाके में आने वाले जिलों में इस वर्ष सूखे के कारण रबी की फसल 70 फीसदी तक बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने केंद्र से किसानों के लिये 205 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक राकेश अगिनहोत्र कहते हैं कि वे और उनकी टीम अप्रैल के पहले सप्ताह महोबा के चरखारी ब्लॉक मेंं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद की प्रतीक्षा करती रही लेकिन एक भी किसान गेहूँ बेचने नहीं आया। ऐसा तब हुआ जब राज्य सरकार ने गेहूँ के लिये 15,250 रुपये प्रति टन का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है। यह दर पिछले साल के मुकाबले 5.2 प्रतिशत अधिक है। वह कहते हैं, “आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हम काफी प्रचार प्रसार के बाद संग्रहण केंद्र का आयोजन करते हैं। अक्सर पहले दिन से ही किसान आने लगते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सूखे की स्थिति काफी गंभीर है। या तो किसानों ने पानी की कमी के कारण पर्याप्त फसल नहीं उपजाई या फिर उत्पादकता बहुत कम रही।” पिछले एक दशक से लगातार फसल का नुकसान हो रहा है और इसके चलते उत्पादन लागत बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है किसान सिंचाई पर अपनी क्षमता से बाहर जाकर खर्च कर रहे हैं।
सूखे के कारण लगातार 15वीं बार फसल खराब हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक बुन्देलखण्ड इलाके में आने वाले जिलों में इस वर्ष सूखे के कारण रबी की फसल 70 फीसदी तक बर्बाद हो गई। राज्य सरकार ने केंद्र से किसानों के लिये 205 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक राकेश अगिनहोत्र कहते हैं कि वे और उनकी टीम अप्रैल के पहले सप्ताह महोबा के चरखारी ब्लॉक मेंं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद की प्रतीक्षा करती रही लेकिन एक भी किसान गेहूँ बेचने नहीं आया। ऐसा तब हुआ जब राज्य सरकार ने गेहूँ के लिये 15,250 रुपये प्रति टन का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रखा है। यह दर पिछले साल के मुकाबले 5.2 प्रतिशत अधिक है। वह कहते हैं, “आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हम काफी प्रचार प्रसार के बाद संग्रहण केंद्र का आयोजन करते हैं। अक्सर पहले दिन से ही किसान आने लगते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सूखे की स्थिति काफी गंभीर है। या तो किसानों ने पानी की कमी के कारण पर्याप्त फसल नहीं उपजाई या फिर उत्पादकता बहुत कम रही।” पिछले एक दशक से लगातार फसल का नुकसान हो रहा है और इसके चलते उत्पादन लागत बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है किसान सिंचाई पर अपनी क्षमता से बाहर जाकर खर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पानी की कमी ने एक नए कारोबार को जन्म दे दिया है। यहाँ कुएँ से पानी खींचकर घरों तक पहुँचाया जा रहा है।
लगातार पड़ रहे सूखे के कारण बहुत बड़ी आबादी यहाँ से दूसरे शहरों में चली गई है। कृषि से आजीविका सुनिश्चित न कर पाने के कारण किसान शहरों में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बांदा के स्वयंसेवी संगठन प्रवास से जुड़े आशीष सागर कहते हैं कि वर्ष 2015 के पोलियो उन्मूलन अभियान के दौरान लगाए गए सरकारी अनुमानों के मुताबिक पिछले 15 साल में करीब 62 लाख लोग बुन्देलखण्ड छोड़कर गए हैं। वह इस रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं।
लगातार पड़ रहे सूखे का एक और प्रभाव आवारा छोड़ दिए गए पशुओं के रूप में सामने आया है। चारा नहीं जुटा पाने के कारण किसान पशुओ को यूँ ही खुला छोड़ देते हैं। समूचे बुन्देलखण्ड क्षेत्र को लेकर कोई आँकड़ा तो उपलब्ध नहीं है लेकिन अकेले चित्रकूट में 3.6 लाख पालतू पशु आवारा घूम रहे हैं। यह पूरे क्षेत्र के पशुओं का 20 फीसदी है। महोबा के अजीमिका जिले की 38 वर्षीय भौरी देवी को श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा क्योंकि इस वर्ष आवारा पशुओं ने उनकी फसल चौपट कर दी। उन्होंने चार हेक्टेयर में से आधे हेक्टेयर पर गेहूँ बोया था क्योंकि सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। वह कहती हैं कि खेती में 50,000 रुपये कर्ज लेकर लगाए थे जिसे अब चुकाना होगा। हालात इतने खराब हैं कि अजनार की ग्राम प्रधान सरोज द्विवेदी हालिया पंचायत चुनावों में इस वादे पर जीत गईं कि वे खेतों को आवारा पशुओं से बचाएंगी। इन इलाकों में जीत का अंतर प्राय: 50 वोट तक रहता है लेकिन वह 1600 वोट से जीतीं। इलाके की बड़ी काश्तकार सरोज कहती हैं,
“चुनाव प्रचार के दौरान ही मेरे पति ने ऐसे 500 पशुओं का ध्यान रखना शुरू कर दिया था और लोगों ने हमारे लिये जमकर मतदान किया।”
न भूलने वाली बर्बादी
 आखिर बुन्देलखण्ड इतने लंबे समय में भी सूखे से निपटने की तैयारी क्यों नहीं कर पाया? उसे तैयारी कर लेनी थी क्योंकि केंद्र ने पिछले एक दशक में जल संरक्षण ढाँचे तैयार करने के लिये 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमेंं 7000 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत सूखे से बचाव के लिये खर्च की गई। इसके अलावा 7266 करोड़ रुपये की राशि केंद्र ने वर्ष 2004 से 2008 तक लगातार चार साल के सूखे के बाद घोषित की थी। 577 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खेती और अन्य संबंधित सेवाओं की मदद के लिये घोषित की थी। इस पूरी राशि को मिलाकर बुन्देलखण्ड में 2006 से 2015 तक यानी 10 साल की अवधि में 1,16,000 जल संरक्षण ढाँचे बनाए गए। इसमेंं 700 चेकडैम और 236 छोटी सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इतने ढाँचों की मदद से पर्याप्त वर्षाजल संरक्षण हो जाना चाहिए था।
आखिर बुन्देलखण्ड इतने लंबे समय में भी सूखे से निपटने की तैयारी क्यों नहीं कर पाया? उसे तैयारी कर लेनी थी क्योंकि केंद्र ने पिछले एक दशक में जल संरक्षण ढाँचे तैयार करने के लिये 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसमेंं 7000 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत सूखे से बचाव के लिये खर्च की गई। इसके अलावा 7266 करोड़ रुपये की राशि केंद्र ने वर्ष 2004 से 2008 तक लगातार चार साल के सूखे के बाद घोषित की थी। 577 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खेती और अन्य संबंधित सेवाओं की मदद के लिये घोषित की थी। इस पूरी राशि को मिलाकर बुन्देलखण्ड में 2006 से 2015 तक यानी 10 साल की अवधि में 1,16,000 जल संरक्षण ढाँचे बनाए गए। इसमेंं 700 चेकडैम और 236 छोटी सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इतने ढाँचों की मदद से पर्याप्त वर्षाजल संरक्षण हो जाना चाहिए था। आखिर बुन्देलखण्ड सूखे से निपटने में क्यों नाकाम रहा इसका उत्तर उन जल संरक्षण ढाँचों में निहित है जो यहाँ बनाए गए। इनमेंं से अधिकांश या तो तकनीकी खामियों के शिकार हैं या परिस्थिति के अनुकूल नहीं हैं। उदाहरण के लिये साकरिया जलाशय की बात करें तो 40 हेक्टेयर में फैला यह जलाशय मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरापुर गाँव में 5.7 करोड़ रुपये की लागत से बना लेकिन यह नाकाम रहा क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पानी जलाशय की ओर आता ही नहीं। हीरापुर निवासी 65 वर्षीय शकरू गोंड कहते हैं कि उन्होंने छह साल पहले जिलाधिकारी से कई बार कहा था कि यह जलाशय कामयाब नहीं होगा क्योंकि पानी बहाव की ढाल दूसरी दिशा में है। यह दलील खारिज कर दी गई क्योंकि इंजीनियरों ने परियोजना को पारित कर दिया था। बहरहाल गाँव वालों की जानकारी ही सही साबित हुई। जलाशय का निर्माण बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत किया गया था ताकि 380 हेक्टेयर इलाके में सिंचाई की जा सके। अब यह बेकार पड़ा है।
 पन्ना जिले में स्थित सकरिया टैंक में पानी इसलिये नहीं इकट्ठा किया जा सका क्योंकि इसकी डिजाइन खराब थी। इसे 5.7 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। शकरू कहते हैं कि जलाशय के लिये जिस जगह का चुनाव किया गया उसके लिये जाति की राजनीति जिम्मेदार है। जलाशय के लिये जिस जगह का सर्वेक्षण किया गया था वह मौजूदा जगह से एक किलोमीटर दूर जमनहारी में स्थित है। वह इलाका काफी नीचा है और वहाँ नेमान और कासेहा नामक जो जलधाराएं हैं वे जलाशय के लिये पानी उपलब्ध करा सकती थीं लेकिन उस जगह की अनदेखी कर दी गई क्योंकि गाँव की रसूखदार जातियों अहीर और ठाकुरों ने इसकी इजाजत नहीं दी। रातों रात जगह बदलने का निर्णय कर लिया गया। जिस जगह पर देश की सबसे गरीब जनजातियों में से एक गोंड रहा करते थे वहाँ जलाशय बनाना शुरू किया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। हर परिवार को मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपये दिए गए। इस जलाशय के लिये अपनी 1.2 हेक्टेयर जमीन गँवाने वाली पान बाई गोंड कहती हैं कि वर्षा का जल भी टैंक में बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहता। यह पानी रिस जाता है और आस-पास के खेतों मेंं फैल जाता है। 60 वर्षीय शंकर गोंड कहते हैं कि उनकी छीनी गई जमीन उर्वर थी लेकिन नई जमीन उर्वर नहीं है।
पन्ना जिले में स्थित सकरिया टैंक में पानी इसलिये नहीं इकट्ठा किया जा सका क्योंकि इसकी डिजाइन खराब थी। इसे 5.7 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था। शकरू कहते हैं कि जलाशय के लिये जिस जगह का चुनाव किया गया उसके लिये जाति की राजनीति जिम्मेदार है। जलाशय के लिये जिस जगह का सर्वेक्षण किया गया था वह मौजूदा जगह से एक किलोमीटर दूर जमनहारी में स्थित है। वह इलाका काफी नीचा है और वहाँ नेमान और कासेहा नामक जो जलधाराएं हैं वे जलाशय के लिये पानी उपलब्ध करा सकती थीं लेकिन उस जगह की अनदेखी कर दी गई क्योंकि गाँव की रसूखदार जातियों अहीर और ठाकुरों ने इसकी इजाजत नहीं दी। रातों रात जगह बदलने का निर्णय कर लिया गया। जिस जगह पर देश की सबसे गरीब जनजातियों में से एक गोंड रहा करते थे वहाँ जलाशय बनाना शुरू किया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। हर परिवार को मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपये दिए गए। इस जलाशय के लिये अपनी 1.2 हेक्टेयर जमीन गँवाने वाली पान बाई गोंड कहती हैं कि वर्षा का जल भी टैंक में बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहता। यह पानी रिस जाता है और आस-पास के खेतों मेंं फैल जाता है। 60 वर्षीय शंकर गोंड कहते हैं कि उनकी छीनी गई जमीन उर्वर थी लेकिन नई जमीन उर्वर नहीं है।पन्ना जिले के गुनौर ब्लॉक में सकरिया से कुछ किलेामीटर दूर एक चकबाँध बनाया गया था। समस्या यह है कि बाँध समतल जमीन पर स्थित है इसलिये पानी कभी अपेक्षित गति हासिल नहीं कर पाता है। बाँध केवल एक बाधा बनकर रह गया है जिसकी वजह से पानी आस-पास के खेतों में फैल जाता है। पन्ना के अमानगंज ब्लॉक के जसवंतपुरा बाँध के साथ मामला एकदम उल्टा है। यह बाँध खराब सामग्री से बना और परिचालन शुरू होने के पहले ही वर्ष इसमेंं दरारें आ गईं। परिणामस्वरूप पानी वहाँ टिकता ही नहीं। अमानगंज ब्लॉक के एक सरकारी शिक्षक डीपी सिंह कहते हैं कि उस बाँध से पूरा पानी बह जाता है।
पन्ना का भितरी मुटमुरु बाँध भी ऐसा ही एक मामला है। वर्ष 2013 में इस बाँध की एक दीवार ढह गई। ऐसा निर्माण कार्य चलने के दौरान ही भारी बारिश के कारण हुआ। पन्ना के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव कहते हैं, “जानकारी के मुताबिक तो कुछ लोग मर भी गए। वह मामला राज्य विधानसभा मेंं भी उठा था। बाँध की मरम्मत का काम गत वर्ष दोबारा शुरू हुआ।”
इस क्षेत्र के प्रत्येक जिले में ऐसी अनगिनत कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। गलत निर्माण ने सदियों पुराने तालाबों को भी नष्ट कर दिया जो कामयाब थे। ऐसा ही एक तालाब महोबा जिले के नागरडांग गाँव में स्थित है जिसका नाम है चाँद सागर। बुंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया यह तालाब सरकार द्वारा आदर्श तालाब घोषित किए जाने के बाद मरणासन्न स्थिति में है। सरकार ने वर्ष 2012-13 में इसे आदर्श तालाब घोषित कर इसकी दशा सुधारने का निर्णय लिया। इसके तहत इसके चारों ओर दीवार बना दी गई और जल भराव क्षेत्र से आने वाला पानी रुक गया।
 गाँव के एक किसान लीलाधर राजपूत मजाकिया लहजे में कहते हैं कि यह तालाब अब अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। यह चाँद की रोशनी मेंं भी सूख सकता है। यह पहल सरकार की उस योजना का हिस्सा थी जिसके तहत हर ब्लॉक मेंं एक आदर्श तालाब बनाना है। कांग्रेस पार्टी की बुन्देलखण्ड राहत पैकेज निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भानु सहाय दावा करते हैं कि पैकेज के तहत दी गई धनराशि पूरी तरह फिजूल खर्च कर दी गई। वह कहते हैं कि राहत पैकेज के तहत खोदे गए तालाबों मेंं से 90 प्रतिशत बेकार हैं।
गाँव के एक किसान लीलाधर राजपूत मजाकिया लहजे में कहते हैं कि यह तालाब अब अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। यह चाँद की रोशनी मेंं भी सूख सकता है। यह पहल सरकार की उस योजना का हिस्सा थी जिसके तहत हर ब्लॉक मेंं एक आदर्श तालाब बनाना है। कांग्रेस पार्टी की बुन्देलखण्ड राहत पैकेज निगरानी कमेटी के अध्यक्ष भानु सहाय दावा करते हैं कि पैकेज के तहत दी गई धनराशि पूरी तरह फिजूल खर्च कर दी गई। वह कहते हैं कि राहत पैकेज के तहत खोदे गए तालाबों मेंं से 90 प्रतिशत बेकार हैं।बांदा के सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से निपटने के लिये खेत तालाब बनाने का अभियान छेड़े हुए हैं।
उपयुक्त विकल्प
मध्ययुगीन समय से ही बुन्देलखण्ड के स्थानीय शासकों और राजाओं ने तालाब बनाए थे। उनमें से कुछ सदियों तक चले और अभी भी कामयाब हैं। पारंपरिक बुद्धिमता यही बताती है कि तालाब इस क्षेत्र के मौसम के लिहाज से बेहतरीन हैं। बांदा के सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं। वह भी इस बात से सहमति जताते हैं। सिंह ने वर्ष 2013 में चंद्रावल नदी के किनारे किनारे 1000 खेत तालाब बनाने का अभियान शुरू किया। बारिश के मौसम में जब नदी उफान पर होगी तो ये तालाब भर जाएंगे और वर्ष के बाकी समय मेंं खेतों को पानी उपलब्ध कराएंगे। सिंह को महोबा के तत्कालीन जिलाधिकारी अनुज झा का समर्थन मिला। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2015 में मनरेगा के तहत की गई।
 इस बीच झा का स्थानांतरण हो गया और योजना में आमूलचूल बदलाव आ गया। अब प्रस्ताव रखा गया है कि पानी का संरक्षण करने के लिये नदी के आस-पास 15 नए चकबाँध बनाए जाने चाहिए। 70 किमी लंबी नदी हमीरपुर और बांदा से होकर बहती है और इस पर पहले ही 5 चेकडैम बन चुके हैं। नाथपुर मेंं बने एक नए चेकडैम में 2 मीटर की दीवार है जो चेकडैम के लिहाज से काफी ऊँची कही जा सकती है। यह पानी के बहाव को बुरी तरह बाधित करती है। इतना ही नहीं इस बाँध के दोनों ओर दो गाँवों कसराई और करहरा कला के नाम लिखे गए हैं ताकि यह झूठा दावा किया जा सके कि गाँवों के लिये दो अलग-अलग चेकडैम बनाए गए हैं। सिंह कहते हैं, “कोई नहीं जानता है कि बाँध पर कितना पैसा खर्च किया गया। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की यही हालत है।”
इस बीच झा का स्थानांतरण हो गया और योजना में आमूलचूल बदलाव आ गया। अब प्रस्ताव रखा गया है कि पानी का संरक्षण करने के लिये नदी के आस-पास 15 नए चकबाँध बनाए जाने चाहिए। 70 किमी लंबी नदी हमीरपुर और बांदा से होकर बहती है और इस पर पहले ही 5 चेकडैम बन चुके हैं। नाथपुर मेंं बने एक नए चेकडैम में 2 मीटर की दीवार है जो चेकडैम के लिहाज से काफी ऊँची कही जा सकती है। यह पानी के बहाव को बुरी तरह बाधित करती है। इतना ही नहीं इस बाँध के दोनों ओर दो गाँवों कसराई और करहरा कला के नाम लिखे गए हैं ताकि यह झूठा दावा किया जा सके कि गाँवों के लिये दो अलग-अलग चेकडैम बनाए गए हैं। सिंह कहते हैं, “कोई नहीं जानता है कि बाँध पर कितना पैसा खर्च किया गया। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की यही हालत है।”अब कन्नौज के जिलाधिकारी बन चुके अनुज झा कहते हैं, “बाँध बनाने के लिये जगह का चुनाव मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।” वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड की बांदा इकाई में इंजीनियर अनिल मिश्रा कहते हैं, “जगह चयन की खातिर अध्ययन हेतु हमसे कभी संपर्क नहीं किया गया। जबकि बाँध बनाने के पहले स्थान विशेष पर पानी के बहाव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नियम के मुताबिक कुल पानी का 35 प्रतिशत चेकडैम से होकर गुजरना ही चाहिए ताकि नदी सदाबहार बनी रहे। शेष 65 फीसदी पानी का प्रयोग किया जा सकता है।” मिश्रा सिंचाई विभाग के इंजीनियरों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं, “वे अपनी अलग योजनाएं बनाते हैं और उनको अमल में लाते हैं जबकि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के मुताबिक तालाब अधिक उपयुक्त हैं।”
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के गोशियारी गाँव के राज मोहम्मद गाँव के इकलौते जल स्रोत की रखवाली बंदूक के सहारे कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं स्नान करती हैं।
हमीरपुर जिले के अतगर गाँव का हीरा तालाब ऐसा ही एक तालाब है। 120 हेक्टेयर में फैले इस तालाब के जल भराव क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया गया है। नतीजा यह कि यह तालाब सदियों से फलफूल रहा है। गाँव के एक निवासी पंचम अराख (58 वर्ष) कहते हैं, “हम नहीं जानते यह कितना पुराना है लेकिन यह कभी नहीं सूखता। यहाँ तक कि इस साल जैसे भीषण सूखे में भी यह बचा रहा।”
सीधा संबंध
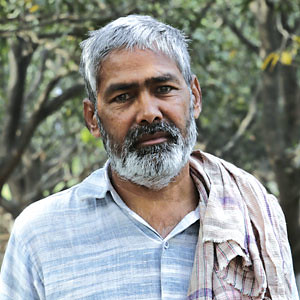 सिंह कहते हैं कि तालाबों के माध्यम से सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था का क्षय सन 1960 के दशक मेंं आरम्भ हुआ जब कई राज्यों मेंं चकबंदी कानून बदले गए। पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो जमीन का मालिकाना पानी की उपलब्धता के हिसाब से था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि हर किसान को खेती के लिये पानी मिले। नए कानून के मुताबिक भूस्वामित्व को चौकोर आकार मेंं काटा गया और पानी की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप किसानों को सिंचाई के अन्य साधनों का रुख करना पड़ा। चकबंदी का असर वर्ष 1990 मेंं महसूस किया गया जब सूखे की समस्या गंभीर हो गई। सिंह कहते हैं, “21वीं सदी मेंं हालात बहुत विकट हो गए हैं। हमने पानी का उपयोग बढ़ा दिया है लेकिन भूजल रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम सतह पर मौजूद पानी को भी बचाने में नाकाम रहे हैं।”
सिंह कहते हैं कि तालाबों के माध्यम से सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था का क्षय सन 1960 के दशक मेंं आरम्भ हुआ जब कई राज्यों मेंं चकबंदी कानून बदले गए। पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो जमीन का मालिकाना पानी की उपलब्धता के हिसाब से था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि हर किसान को खेती के लिये पानी मिले। नए कानून के मुताबिक भूस्वामित्व को चौकोर आकार मेंं काटा गया और पानी की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप किसानों को सिंचाई के अन्य साधनों का रुख करना पड़ा। चकबंदी का असर वर्ष 1990 मेंं महसूस किया गया जब सूखे की समस्या गंभीर हो गई। सिंह कहते हैं, “21वीं सदी मेंं हालात बहुत विकट हो गए हैं। हमने पानी का उपयोग बढ़ा दिया है लेकिन भूजल रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम सतह पर मौजूद पानी को भी बचाने में नाकाम रहे हैं।”किसान सिंचाई के लिये अन्य तरीकों का रुख करने लगे और पारंपरिक जल स्रोतों की अनदेखी की जाने लगी जिससे वे बेकार हो गए। सन 1983 मेंं मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण की एक रिपोर्ट मेंं कहा गया कि इस इलाके मेंं 9,407 तालाब हैं। बांदा के गैर सरकारी संगठन विज्ञान संचार संस्थान की रिपोर्ट मेंं कहा गया कि सन 1990 तक बुन्देलखण्ड के उत्तर प्रदेश में आने वाले इलाके मेंं 11,000 तालाब थे जो अब बमुश्किल 5500 बचे हैं। सिंह कहते हैं कि बुन्देलखण्ड मेंं बढ़ते जल संकट और जलाशयों की कमी मेंं सीधा संबंध है।
महोबा का मदन सागर ताल मृतप्राय हो रहा है क्योंकि इसके जल भराव क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया गया है। इतना ही नहीं इसमेंं तमाम जगह की गंदगी भी आकर मिलती है।
झांसी के भूविज्ञानी नरेंद्र गोस्वामी कहते हैं कि इस इलाके की भौगोलिक बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यह बहुत जल्दी पानी को अवशोषित भी करता है व इसकी निकासी भी तेज होती है। यही वजह है कि तालाब यहाँ जल संरक्षण के लिये बहुत अच्छा जरिया हैं। यहाँ भूजल का दोहन कतई मददगार नहीं हो सकता। झांसी के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण गाँधी ने लोकोद्यम संस्थान की शुरुआत की थी। वे कहते हैं कि बुन्देलखण्ड मेंं भूजल स्रोत बहुत कम हैं क्योंकि यहाँ ग्रेनाइट व शैल चट्टानें हैं जो बहुत सख्त होती हैं। इनके कारण पानी रिस नहीं पाता। वहीं, दूसरी तरफ बुन्देलखण्ड मेंं सतह के नीचे मौजूद स्फटिक की लहरदार चट्टानें तालाब बनाने के लिये उपयुक्त माहौल देती हैं। उनका संस्थान क्षेत्र मेंं जल संरक्षण के लिये काम करता है। गाँधी कहते हैं कि करीब 1000 साल पहले चंदेल शासकों ने इन चट्टानों के बीच जो तालाब बनाए थे वे आज भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के पत्रकार पंकज चतुर्वेदी जिन्होंने बुन्देलखण्ड मेंं पारंपरिक जल संरक्षण साधनों पर दो पुस्तकें लिखी हैं, वह कहते हैं कि जब तक यह नहीं होता तब तक यह इलाका सूखे से निपटने के लिये तैयार नहीं होगा।
Path Alias
/articles/paayaa-kama-khaoyaa-jayaadaa
Post By: Hindi