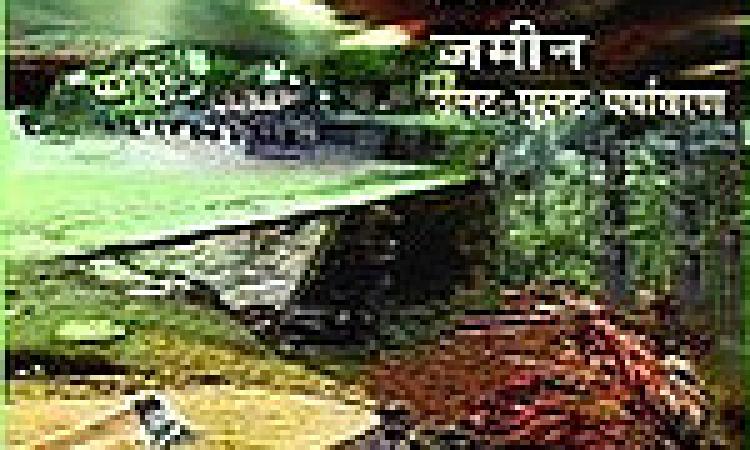
हिमालय की लगभग 2,400 किलोमीटर की तराई वाली पट्टी में लोगों में घेंघा की शिकायतें पाई जाती थीं। इसके अलावा कुछ जल जमाव वाले क्षेत्रों में इसकी पहचान की गई थी, परन्तु अन्य जगहों में आयोडीन की जरूरत वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों कुओं के जल, भूजल, हरी साग-सब्जियों आदि से पूरी हो जाती है। फिर सरकार उन क्षेत्रों में भी आयोडीन नमक क्यों जबरन खिलाना चाहती है?
हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली महानगर में भी घेंघा जैसे रोग का प्रचलन बढ़ रहा है। इसका कारण आयोडीन की कमी नहीं है, बल्कि डेयरी, गाय और भैंस के दूध में थायोसाइनेट नामक एक तत्व अलग से मिलाने से ऐसा हो रहा है।
थायोसाइनेट का काम दूध को ताजा बनाए रखना होता है। दूध उबालने के क्रम में थायोसाइनेट पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता है। प्राकृतिक तौर पर साधारण दूध में थायोसाइनेट प्रतिलीटर 10-20 मिलीग्राम तक प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है। प्रिजरवेटिव के रूप में इसका अलग से इस्तेमाल शरीर के लिये अत्यधिक नुकसानदेह हो जाता है। यह तथ्य पहले भी 1987 में स्कूली बच्चों के बीच हुए एक सर्वेक्षण के दौरान प्रकट हुए थे। सर्वेक्षण के अन्तर्गत चौंकाने वाले तथ्य सामने आये थे, जो पहले प्रकाशित किये जा चुके हैं। गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से प्रकाशित पुस्तक ‘हमारा पर्यावरण’ में ज्योति प्रकाश अपने लेख में लिखते हैं, ‘सन 87 में दिल्ली के स्कूली बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि साधारण स्कूलों की अपेक्षा अमीर स्कूलों के बच्चों में घेंघा के लक्षण ज्यादा मिले हैं, यानी जो ज्यादा दूध पीते हैं, वे इसके ज्यादा शिकार होंगे। हालांकि समय-समय पर बदलती सरकारों ने घेंघा का कारण आयोडीन की कमी बताकर, साधारण नमक पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश भी की है।
आयोडीन की कमी से घेंघा की बीमारी होती है, यह सत्य है, परन्तु, घेंघा की शिकायत शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी से और सबसे बड़ी बात है कि भोजन के अभाव में और तीव्रता के साथ प्रकट होती है। वर्तमान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से सहयोग लेकर इसे लगभग 125 करोड़ लोगों पर थोपने की जबरन कोशिश शुरू कर दी है। 1987 से लेकर 18 सालों तक के इस लम्बे अन्तराल में आती-जाती सरकारों ने दूध में हो रही मिलावटों पर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात यह कि वह कभी भी दूध में मिलावट से घेंघा जैसी बीमारी का प्रचलन बढ़ने की बात बताती तक नहीं है। वह इन 18 सालों के लम्बे अन्तराल में दूध में मिलावट को क्यों नहीं दूर कर पाई? सरकार साधारण नमक पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये एक पक्ष को ही सामने लाती है। वह दूसरे पक्ष पर चुप्पी साध लेती है। दरअसल एक तरफ डेयरी से जुड़े उद्योगपतियों का दबाव है तो दूसरी ओर पैकेट बन्द आयोडीन नमक के कारोबार में लगभग 2,500 करोड़ के मुनाफे का बाजार का दोहन करने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित से जुड़ा हुआ है। सरकार अपने दबाव को हल्का करने के लिये कोई जनपक्षीय रास्ता न निकालकर, बल्कि सारा दबाव आम जनता पर डाल देती है, क्योंकि वह नीतियों के निर्धारण में अपना हित भी देखती है। इसकी पड़ताल जरूरी है।
दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण विभाग ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में बेचे जा रहे खुले व पैकेट वाले दूध के नमूनों की जाँच की थी। इसमें कई नामी-गिरामी डेयरियों की तीनों किस्म और गाय, भैंस के खुले दूध के नमूनों की जाँच की थी। इसमें कई नामी-गिरामी डेयरियों के तीन आँकड़ों के अनुसार मिलावटी दूध बेचने की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। वर्ष 2004 में दूध के कुल 148 नमूनों में 126 में मिलावट पाई गई थी। वर्ष 2003 में 231 नमूनों की जाँच में 41 नमूनों में मिलावट पाई गई थी। आँकड़ों के हिसाब से यह मिलावट लगभग 25 फीसदी के आसपास है। मिलावट बाजार की आदतों में शामिल रही है। अकारण नहीं है कि छठे दशक के फिल्मी नायक पर ‘खाली डब्बा, खाली बोतल’ जैसे गाने फिल्माए गए। मिलावट के आयोडीनयुक्त नमक पर घालमेल को और सलीके से पुष्ट करता प्रतीत होता है। वास्तविकता तो यह है कि आयोडीनयुक्त नमक, जिसके प्रचार-प्रसार में सरकार अपनी पूरी ताकत से लगी है, वह भी आधे सच को ही स्थापित करता है। नमक में आयोडीन की जगह पोटेशियम आयोडेड मिलाया जा रहा है, जिस पर दूसरे देशों ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसकी वजह यह थी कि पोटेशियम आयोडेड एक जहरीला पदार्थ है, जो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाता है।
हिमालय की लगभग 2,400 किलोमीटर की तराई वाली पट्टी में लोगों में घेंघा की शिकायतें पाई जाती थीं। इसके अलावा कुछ जल जमाव वाले क्षेत्रों में इसकी पहचान की गई थी, परन्तु अन्य जगहों में आयोडीन की जरूरत वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों कुओं के जल, भूजल, हरी साग-सब्जियों आदि से पूरी हो जाती है। फिर सरकार उन क्षेत्रों में भी आयोडीन नमक क्यों जबरन खिलाना चाहती है? इसका मतलब तो यह हुआ कि हम क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे, यह अब सरकार असंवैधानिक तरीके से तय करेगी, क्योंकि संविधान हमें इन बातों की पूरी आजादी देता है।
सरकार को जनहित के लिये खाद्य सामग्री की शुद्धता के लिये जो कठोर निर्णय लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। सरकार ने पिछले 18 सालों में दूध जैसे पोषक तत्वों में मिलावट से अपनी नजरें हटाकर अपने जनपक्षीय होने के दावे को झुठलाया है। यह मामला दूध से जुड़े उन स्कूली बच्चों के प्रति जघन्यतम अपराधों में से एक है, जिस पर वह अपने तमाम प्रचार माध्यमों के साथ चुप्पी साधना ही बेहतर समझती है। पिछले दिनों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में संस्थान के ही 200 से ज्यादा चिकित्सकों के लगातार विरोध के बाद भी सेवा शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गई। सरकार के जनपक्षीय होने के ढोंग के जगजाहिर होने का इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। छठे व सातवें दशक में ऐसी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनसंगठन, जनता, साहित्य और सिनेमा, सभी जगह विरोध के तेवर ज्यादा तीखे दिखते हैं। इन विरोधों का सरकार पर नैतिक दबाव भी काम करता था, लेकिन अब जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर से नैतिकता का बोझ कम हो गया है।
|
जल, जंगल और जमीन - उलट-पुलट पर्यावरण (इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को पढ़ने के लिये कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें) |
|
|
क्रम |
अध्याय |
पुस्तक परिचय - जल, जंगल और जमीन - उलट-पुलट पर्यावरण |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
/articles/badae-saharaon-maen-ghaenghaa-kae-badhatae-khatarae